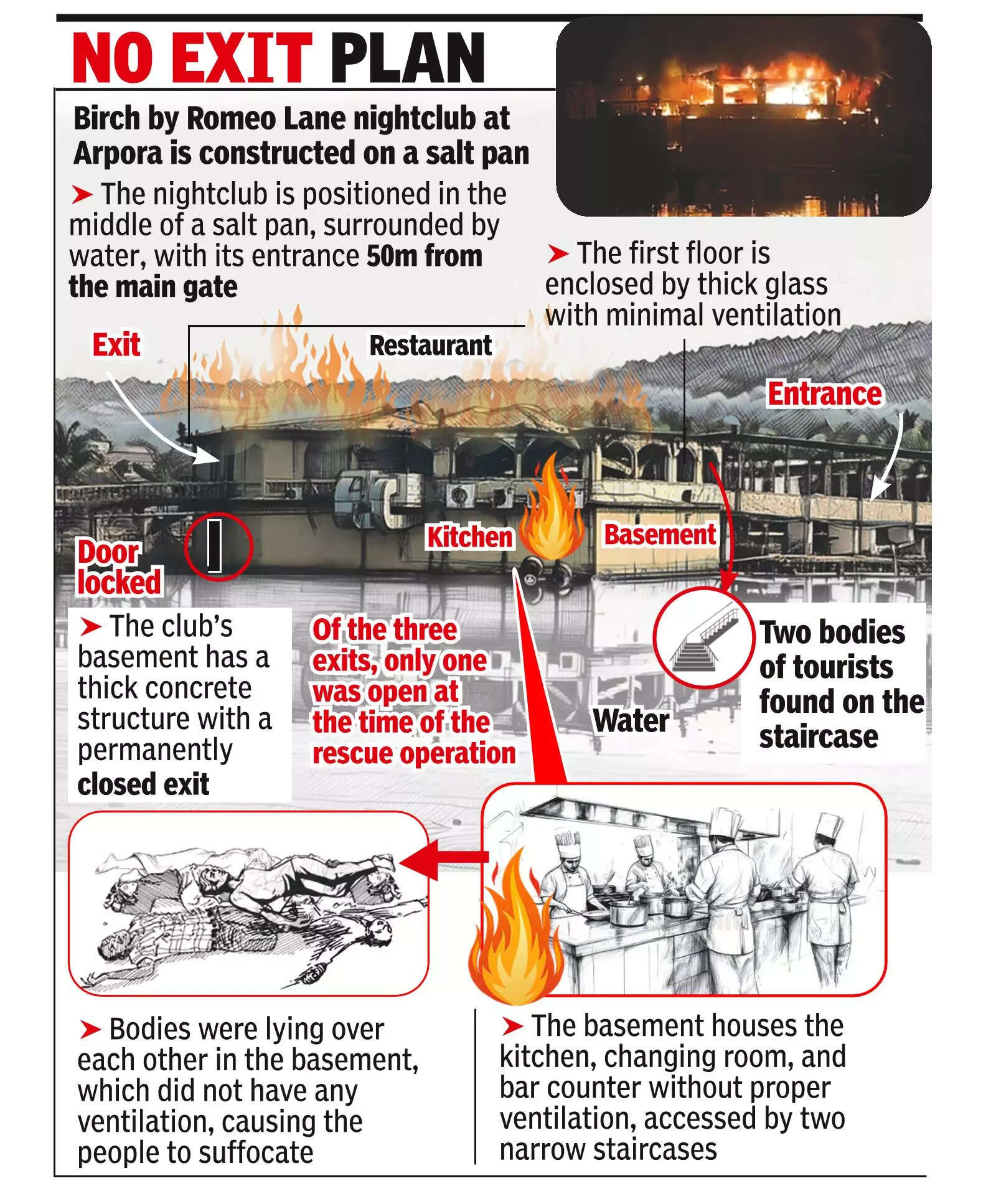पटना: बैलगाड़ी के इस्तेमाल से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक, 1952 में पहले आम चुनाव होने के बाद से बिहार में चुनाव प्रचार में व्यापक बदलाव देखा गया है। तकनीकी नवाचारों की लगातार बढ़ती प्रगति के साथ, दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में भी प्रतियोगियों के लिए प्रचार करना काफी आसान हो गया है। आज चुनाव व्यस्त, ज़ोरदार घर-घर प्रचार के आधार पर नहीं, बल्कि मुख्य रूप से डिजिटल आउटरीच और सोशल मीडिया की मदद से लड़े जाते हैं।लेकिन क्या चुनाव के नतीजे केवल उम्मीदवारों और उन पार्टियों द्वारा अपनाए गए प्रचार के तरीके पर निर्भर करते हैं जिनसे वे संबंधित हैं? चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारक क्या हैं? क्या बिहार के मतदाता उसी पुराने पैटर्न पर वोट डालते रहेंगे या वे 2025 में व्यवस्था में कुछ बदलाव चाहेंगे?
आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के मूड पर सामाजिक वैज्ञानिकों की अलग-अलग राय है। जबकि, कुछ का मानना है कि बिहार में जाति अभी भी एक सामाजिक वास्तविकता बनी हुई है और अधिकांश राजनीतिक दल, विशेष रूप से क्षेत्रीय दल, जाति समूहों के आसपास बने हैं। दूसरों को लगता है कि मतदाताओं का व्यवहार रोज़गार और आवश्यक वस्तुओं की कीमत जैसे ‘पॉकेटबुक’ मुद्दों से प्रभावित होता है। उनका कहना है कि आर्थिक प्रदर्शन और कल्याणकारी योजनाओं का वादा मतदाताओं को विभिन्न जातिगत आधारों पर प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं।बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के एसोसिएट प्रोफेसर सुधांशु कुमार ने बताया कि आज के डिजिटल युग में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वायरल मीम्स, लघु वीडियो और ट्रेंडिंग हैशटैग द्वारा चुनावी चर्चा को नया आकार दिया जा रहा है। यह बदला हुआ माहौल राजनीतिक दलों के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, बिहार में, 2005 से 2025 तक मतदाताओं में 41% की वृद्धि ने राज्य में प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की औसत संख्या 2.2 लाख से बढ़ाकर 3.1 लाख कर दी, जिससे भौतिक पहुंच कठिन हो गई। उन्होंने कहा, बढ़ी हुई सेलफोन पहुंच और किफायती इंटरनेट ने संचार में क्रांति ला दी है, जिससे अभियान की पहुंच बढ़ गई है।जैसे-जैसे अभियान तेजी से परंपरा और नवीनता का मिश्रण कर रहे हैं, मतदाताओं को नीतिगत सार और बयानबाजी के बीच अंतर करने की आवश्यकता होगी। कुमार ने कहा, हालांकि जाति और धर्म-आधारित विभाजनकारी एजेंडे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जारी हैं, शिक्षा और करियर को प्राथमिकता देने वाली आकांक्षी युवा पीढ़ी धीरे-धीरे अपने प्रभाव को कम कर सकती है, अंततः अधिक सूचित विकल्पों के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है।आईआईटी-पटना में सामाजिक विज्ञान और मानविकी के एसोसिएट प्रोफेसर, आदित्य राज ने पाया कि बिहार के मतदाता एक समान या समरूप नहीं हैं। चुनाव अभियान शायद ही ‘कैडर’ मतदाताओं (राजनीतिक दलों के सदस्य या कार्यकर्ता) या ‘अदूरदर्शी’ मतदाताओं के लिए मायने रखते हैं, जिन्हें आमतौर पर अपनी जाति या समुदाय के लिए वोट देने का लालच दिया जाता है। ‘फ़्लोटिंग’ मतदाता चुनाव अभियानों, बहसों में वादों पर नज़र रखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। ये मतदाता राय बनाने वालों से प्रभावित होते हैं और अक्सर वे अपने सहयोगियों और पड़ोस को भी प्रभावित कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा, “नई पीढ़ी”, जो ज्यादातर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, वास्तविक परिवर्तन निर्माता हैं।एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर विद्यार्थी विकास ने कहा कि आधुनिक राजनीतिक अभियानों को आम तौर पर “उम्मीदवार-केंद्रित” के रूप में देखा जाता है और मात्रात्मक विश्लेषण में इसे सशर्त रूप से स्वतंत्र माना जाता है। हालाँकि, ये अभियान पेशेवर परामर्श फर्मों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं, जो समकालीन युग के विस्तारित पार्टी नेटवर्क के भीतर अभियान रणनीतियों को फैलाने में प्रमुख एजेंटों के रूप में काम करते हैं। पिछले एक दशक में राजनीतिक विज्ञापन में काफी बदलाव आया है, यह घर-घर जाकर प्रचार करने या सार्वजनिक रैलियों जैसे पारंपरिक तरीकों से हटकर डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ गया है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से राज्य में नई चुनावी राजनीति को एक नया आयाम मिलने की संभावना है।